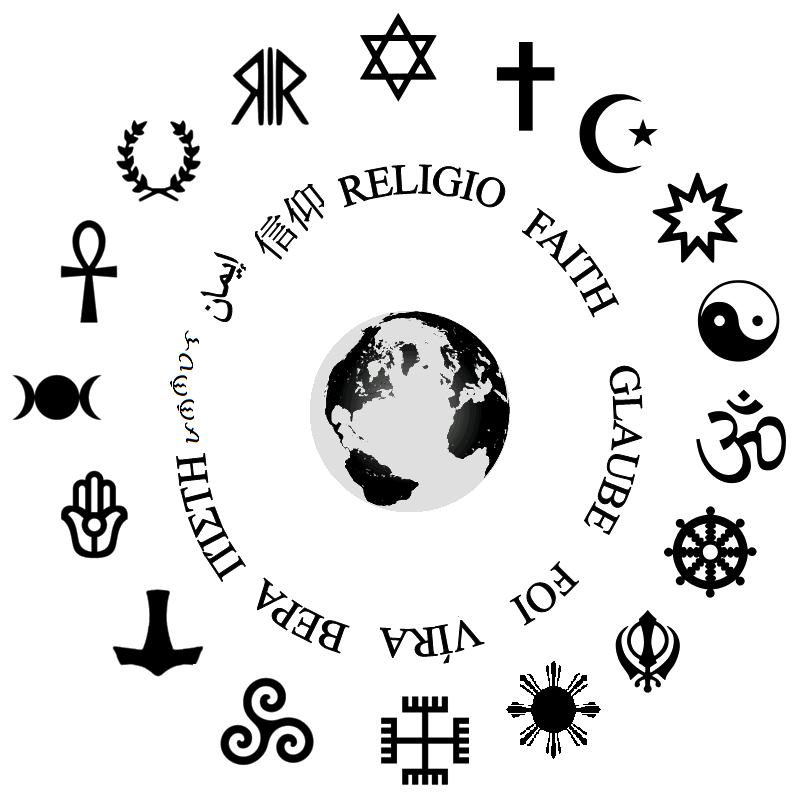मोर्चा पत्रिका के लिए अनूदित (ड्राफ्ट)
[जर्मनी की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी क्लारा ज़ेटकिन (1857-1933) ने जून 1923 में कॉमिन्टर्न की कार्यकारिणी समिति के तीसरे अभिवर्धित प्लेनम में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट अंग्रेजी में ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की मासिक पत्रिका, लेबर मंथली, में अगस्त 1923 में संक्षेप में छपी थी, जिसका यहाँ हम हिन्दी अनुवाद दे रहे हैं। इससे पहले नवंबर 1922 में इतालवी मार्क्सवादी अमादेओ बोर्दीगा ने भी फासीवाद पर एक रिपोर्ट कॉमिन्टर्न में पेश की थी, परंतु ज़ेटकिन की रिपोर्ट ने ही फासीवाद पर बाद की कम्युनिस्ट समूहों की चर्चाओं के लिए प्रथम व्यवहारात्मक-आलोचनात्मक दृष्टिकोण तैयार किया था।
इस रिपोर्ट में ज़ेटकिन फासीवाद के उत्थान को पूंजीवाद के आर्थिक संकट और उसके संस्थाओं के पतन से जोड़ती हैं। मजदूर वर्ग पर बढ़ता आक्रमण और अन्य वर्गों का सर्वहाराकरण इस संकट के प्रमुख नतीजे हैं। ज़ेटकिन का मानना है कि सत्तासीन होकर समाज को पुनर्गठित कर पूंजीवाद के सामाजिक संकट का निवारण करने में सर्वहारा वर्ग की असफलता फासीवाद को जन्म देती है। पूंजीवाद के संकट से व्याकुल हो रहे विभिन्न निम्न-पूंजीवादी तबकों को आकर्षित करने की क्षमता फासीवाद को जन-चरित्र देती है। फासीवादी विचारधारा राष्ट्र और राजसत्ता को वर्गीय अंतर्विरोधों और हितों से ऊपर रख अंध-राष्ट्रवाद फैला कर सैन्यवाद और युद्धवाद के लिए माहौल तैयार करती है। पूंजीपति वर्ग के कई महत्वपूर्ण तबके पूंजीवाद के सामान्य संकट और जनता के लगातार सर्वहाराकरण के कारण अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्वता पर खतरे से बचने के लिए फासीवाद का समर्थन और वित्तीय पोषण आरंभ कर देते हैं।
ज़ेटकिन फासीवाद पर ओटो बावर (जो कि ऑस्ट्रीया के सामाजिक-जनवादी पार्टी के प्रमुख नेता और सिद्धांतकार थे) जैसे सुधारवादियों की समझ की तीव्र आलोचना करती हैं, ओटो बावर के अनुसार फासीवाद महज कम्युनिस्टों द्वारा संगठित सर्वहारा लड़ाकूपन और कानूनेतर गतिविधियों का नतीजा था। ज़ेटकिन फासीवाद के खिलाफ शोषित जनता के अपने रक्षा पहलों पर जोर देती हैं। उनके अनुसार सर्वहारा वर्गीय संयुक्त मोर्चे का निर्माण ही फासीवाद को चुनौती दे सकता है। परंतु यह संघर्ष राजनीतिक और वैचारिक भी है इनके द्वारा श्रमिक वर्ग को मध्यम वर्गीय तबकों तक अपनी पहुँच बनानी होगी चूंकि इनके ऊपर पूंजीवादी संकट और सर्वहाराकरण का असर पड़ता है। ज़ेटकिन के अनुसार मजदूरों और किसानों की संयुक्त सरकार ही सामाजिक-आर्थिक संकट का निवारण कर फासीवाद का विनाश कर सकती है।
हमारी दृष्टि में क्लारा ज़ेटकिन की यह रिपोर्ट केवल ऐतिहासिक महत्व नहीं रखती है। जहां तक फ़ासिज़्म के खिलाफ तात्कालिक रणनीतियों का सवाल है वह तो स्थान और समय के मुताबिक तब्दील होती रहती हैं। परंतु इस रिपोर्ट में निहित मार्क्सवादी व्याख्यात्मक अंतर्दृष्टि आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। फासीवाद को महज सत्ता के औजार के बने बनाए रूप में न देख उसको सामाजिक प्रक्रियाओं और वर्ग सघर्षों की अवस्थाओं के अंदर से पनपता हुआ देखने की जरूरत है। आज पिछले पाँच दशकों से वैश्विक पूंजीवादी राजनीतिक अर्थतन्त्र स्थायी-संकट से ग्रस्त है। इस संकट से निज़ात पाने के लिए भूमंडलीय वित्तीयकरण की प्रक्रिया लगातार बृहत्तर और तीव्रतम होती जा रही। विडंबना यह है कि इस प्रक्रिया ने आर्थिक-सामाजिक संकट को और अधिक व्यापक और तीव्र कर दिया है, यहां तक कि विश्व की तमाम राजसत्ताएँ इसके कारण निरंतर वैधता के संकट में डूबती जा रही हैं — इनकी आक्रामकता इनकी बढ़ती असंगतता और कमज़ोरियों के लक्षण हैं। इसी संकटावस्था को सकारात्मक भाषा में नवोदरवाद भी कहते हैं। यह तथ्य इस रिपोर्ट की अंतर्दृष्टि को और महत्व दे देता है क्योंकि फासीकरण इस अवस्था में समूचे सामाजिक-राजनीतिक संरचना में गुत्थ गई है, और इसके खिलाफ संघर्ष को तात्कालिकवाद में सीमित नहीं रखा जा सकता । ]
फासीवाद के रूप में, सर्वहारा वर्ग का सामना एक असाधारण खतरनाक शत्रु से होता है। फासीवाद सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध विश्व पूंजीपति वर्ग द्वारा किये गये व्यापक आक्रमण की घनीभूत अभिव्यक्ति है। इसलिए इसे उखाड़ फेंकना नितांत आवश्यक ही नहीं, बल्कि यह हर साधारण श्रमिक की रोजमर्रा की ज़िंदगी और रोजी-रोटी का सवाल भी है। इन्हीं आधारों पर समूचे सर्वहारा वर्ग को फासीवाद के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम स्पष्टता और गहनता से इसकी प्रकृति का अध्ययन करें तो फासीवाद को हराना हमारे लिए बहुत आसान होगा। अब तक इस विषय पर न केवल श्रमिकों के विशाल जनसमूह के बीच, बल्कि सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी अग्रदूतों और कम्युनिस्टों के बीच भी बेहद अस्पष्ट विचार रहे हैं। अब तक फासीवाद को हंगरी में होर्थी (Horthy) के श्वेत आतंक के समकक्ष समझा गया है। हालाँकि दोनों की पद्धतियाँ समान हैं, लेकिन मूलतः वे अलग-अलग हैं। होर्थी आतंक सर्वहारा वर्ग की विजयी, अपितु अल्पकालिक, क्रांति को दबा दिए जाने के उपरांत स्थापित हुआ था, और यह पूंजीपति वर्ग के प्रतिशोध की अभिव्यक्ति थी। श्वेत आतंक का सरगना पूर्व अधिकारियों का एक छोटा सा गुट था। इसके विपरीत, वस्तुपरक रूप से देखा जाए तो फासीवाद, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सर्वहारा आक्रामकता के प्रतिशोध में पूंजीपति वर्ग का बदला नहीं है, बल्कि वह रूस में शुरू हुई क्रांति को जारी रखने में विफल रहने के लिए सर्वहारा वर्ग की सजा है। फासीवादी नेताओं की कोई छोटी और विशिष्ट जाति नहीं है; वे जनसंख्या के व्यापक हिस्सों में गहराई से फैले हुए हैं।
केवल सैन्य रूप से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक रूप से भी हमें फासीवाद पर काबू पाना होगा। आज भी सुधारवादियों के लिए फासीवाद नग्न हिंसा — सर्वहारा वर्ग द्वारा शुरू की गई हिंसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया — के अलावा कुछ भी नहीं है। सुधारवादियों के लिए रूसी क्रांति अदन की वाटिका में हव्वा के सेब चखने [यानि महापाप] के समान है। सुधारवादी फासीवाद को रूसी क्रांति और उसके परिणामों से जोड़ते हैं। हामबुर्ग के एकता सम्मेलन में ओटो बावर का इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं था, जब उन्होंने फासीवाद के लिए बहुत हद तक दोषी कम्युनिस्टों को ठहराया, जिन्होंने, उनके अनुसार, लगातार विभाजन से सर्वहारा वर्ग की ताकत को कमजोर कर दिया था। यह कहते हुए उन्होंने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि रूसी क्रांति के इस मनोबल गिराने वाले उदाहरण से बहुत पहले जर्मनी के स्वतंत्र [सामाजिक-जनवादियों] ने विभाजन को अंजाम दिया था। खुद के विचारों के विपरीत, बावर को हामबुर्ग में इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि फासीवाद की संगठित हिंसा का मुकाबला सर्वहारा वर्ग के रक्षा संगठनों के निर्माण से किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष हिंसा के खिलाफ लोकतंत्र की कोई भी अपील काम नहीं कर सकती। अवश्य ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनका मतलब विद्रोह या आम हड़ताल जैसे हथियारों से नहीं था जिनसे हमेशा सफलता नहीं मिली है। उनका अभिप्राय जन कार्रवाई के साथ संसदीय कार्रवाई के सामंजस्य से था। ओटो बावर ने यह नहीं बताया कि इन कार्रवाइयों की प्रकृति क्या होगी, जबकि प्रश्न का मूल बिंदु यही है। फासीवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एकमात्र हथियार जिसकी सिफारिश बावर ने की वह विश्व प्रतिक्रियावाद पर अंतर्राष्ट्रीय सूचना ब्यूरो की स्थापना थी। इस नए-पुराने इंटरनेशनल का विशिष्ट लक्षण पूंजीवादी वर्चस्व की शक्ति और स्थायित्व में उसका विश्वास और विश्व क्रांति के सबसे मजबूत कारक के रूप में सर्वहारा वर्ग के प्रति उसका अविश्वास और बुज़दिली है। उसका मानना है कि सर्वहारा पूंजीपति वर्ग की अजेय ताकत के खिलाफ संयम से काम लेने और पूंजीपति वर्ग के बाघ को छेड़ने से परहेज करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।
वास्तव में, अपने हिंसक कृत्यों के अभियोजन में अपनी पूरी ताकत के साथ, फासीवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विघटन और क्षय की अभिव्यक्ति और बुर्जुआ राजसत्ता के भंग होने के लक्षण के अलावा और कुछ नहीं है। यही उसके आधारों में से एक है। पूंजीवाद के इस पतन के लक्षण युद्ध से पहले ही दिखाई देने लगे थे। युद्ध ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उसकी नींव समेत तहस-नहस कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप न केवल सर्वहारा वर्ग में भारी दरिद्रता आई है, बल्कि निम्न पूंजीवादी वर्ग, छोटे किसानों और बुद्धिजीवियों की भी बड़ी दुर्गति हुई है। इन सभी समूहों से वादा किया गया था कि युद्ध से उनकी भौतिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत — बड़ी संख्या में पहले का मध्यम वर्ग अपनी आर्थिक सुरक्षा को पूरी तरह से खोकर सर्वहारा बन गया है। इस कतार में बड़ी संख्या में पूर्व अधिकारी भी शामिल हो गए, जो अब बेरोजगार हैं। इन्हीं तत्वों में से फासीवाद को अपने लिए पर्याप्त रंगरूट मिले। फासीवाद की ऐसी संरचना कई देशों में उसके मुखर राजशाहीवादी चरित्र का कारण है।
फासीवाद की दूसरी जड़ सुधारवादी नेताओं के विश्वासघाती रवैये द्वारा विश्व क्रांति की गति को धीमा करने में निहित है। सुधारवादी समाजवाद के प्रति निश्चित सहानुभूति की वजह से और इस आशा में कि वह लोकतांत्रिक तर्ज पर समाज में सुधार लाएगा बड़ी संख्या में निम्न पूंजीपति वर्ग ने, यहां तक कि माध्यम वर्ग ने भी, युद्ध काल की अपनी मनोवृत्ति को त्याग दिया था। वे निराश थे। उन्हें दिख रहा है कि सुधारवादी नेता पूंजीपति वर्ग के साथ एक परोपकारी समझौते में हैं। इससे भी बुरा यह है कि इस जनता ने अब न केवल सुधारवादी नेताओं में, बल्कि समग्र रूप से समाजवाद में भी अपना विश्वास खो दिया है। समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वालों की इस निराश भीड़ में सर्वहारा वर्ग का बड़ा हिस्सा भी शामिल हो गया है – उन श्रमिकों का, जिन्होंने न केवल समाजवाद में, बल्कि अपने वर्ग में भी अपना विश्वास छोड़ दिया है। फासीवाद राजनीतिक रूप से आश्रयहीन लोगों के लिए एक प्रकार की शरणस्थली बन गया है। निष्पक्षता में यह भी स्वीकारा जाना चाहिए कि कम्युनिस्ट भी – रूसियों को छोड़कर – फासीवादी कतारों में इन तत्वों के पलायन के लिए कुछ हद तक दोषी हैं, क्योंकि कई बार हमारी कार्रवाइयाँ जनता को गहराई से आंदोलित करने में विफल रही हैं। समाज के विभिन्न तत्वों के बीच समर्थन प्राप्त करते समय फासीवादियों का स्पष्ट उद्देश्य, निश्चित रूप से, अपने अनुयायियों के बीच वर्ग विरोध को पाटने का प्रयास करना रहा होगा और तथाकथित आधिकारिक राज्य को इस उद्देश्य के लिए एक साधन के रूप में काम करना था। फासीवाद अब ऐसे तत्वों को गले लगाता है जो पूंजीवादी व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। फिर भी, अब तक इन तत्वों पर प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने लगातार विजय प्राप्त की है।
पूंजीपति वर्ग ने शुरू से ही स्थिति को स्पष्ट रूप से देख लिया था। वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना चाहता है। वर्तमान परिस्थितियों में पूंजीपति वर्ग के वर्चस्व का पुनर्निर्माण पूंजीपति वर्ग द्वारा केवल सर्वहारा वर्ग के बढ़ते शोषण की कीमत पर ही किया जा सकता है। पूंजीपति वर्ग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि मृदुभाषी सुधारवादी समाजवादी सर्वहारा वर्ग पर अपनी पकड़ तेजी से खो रहे हैं, और पूंजीपति वर्ग के लिए सर्वहारा वर्ग के खिलाफ हिंसा का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन पूंजीवादी राज्यों के हिंसा के साधन विफल होने लगे हैं। इसलिए उन्हें हिंसा के नए संगठन की आवश्यकता है, और यह उन्हें फासीवाद का खिचड़ी समूह मुहैया कराता है। इस कारण से पूंजीपति वर्ग फासीवाद की सेवा में अपनी सारी ताकत लगा देता है।
विभिन्न देशों में फासीवाद की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। फिर भी इसकी दो विशिष्टताएं सभी देशों में समान रूप से मौजूद होती हैं — एक, क्रांतिकारी कार्यक्रम का दिखावा, जिसे चतुराई से बड़े पैमाने पर जनता के हितों और मांगों के लिए अनुकूलित किया जाता है, और दूसरी ओर, सबसे क्रूर हिंसा का प्रयोग। इसका उत्कृष्ट उदाहरण इतालवी फासीवाद है। इटली में औद्योगिक पूंजी इतनी मजबूत नहीं थी कि बर्बाद अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर सके। यह उम्मीद नहीं थी कि राजसत्ता उत्तरी इटली की औद्योगिक राजधानी की शक्ति और भौतिक संभावनाओं के विस्तार के लिए हस्तक्षेप करेगी। राज्य अपना सारा ध्यान कृषि पूंजी और छोटी वित्तीय पूंजी पर दे रहा था। भारी उद्योग, जिन्हें युद्ध के दौरान कृत्रिम रूप से बढ़ावा दिया गया था, युद्ध समाप्त होने पर ध्वस्त हो गए और अभूतपूर्व बेरोजगारी की लहर चल पड़ी। सैनिकों को दिए गए वादे पूरे नहीं किए जा सके। इन सभी परिस्थितियों ने अत्यंत क्रांतिकारी माहौल को जन्म दिया। इस क्रांतिकारी माहौल के परिणामस्वरूप, 1920 की गर्मियों में, कारखानों पर कब्ज़ा हो गया। उस अवसर पर क्रांति की परिपक्वता सर्वहारा वर्ग के एक छोटे से अल्पसंख्यक हिस्से के बीच पहली बार प्रकट होती हुई दिखी। इसलिए फ़ैक्टरियों पर कब्ज़ा क्रांतिकारी विकास का शुरुआती बिंदु बनने के बजाय एक ज़बरदस्त हार के साथ ख़त्म होना तय था। ट्रेड यूनियनों के सुधारवादी नेताओं ने घृणित गद्दारों की भूमिका निभाई, लेकिन साथ ही यह भी दिखा कि सर्वहारा वर्ग के पास क्रांति की ओर बढ़ने की न तो इच्छा थी और न ही शक्ति।
सुधारवादी प्रभाव के बावजूद, सर्वहारा वर्ग के बीच ऐसी ताकतें काम कर रही थीं जो पूंजीपति वर्ग के लिए असुविधाजनक हो सकती थीं। नगरपालिका चुनाव, जिसमें सामाजिक जनवादियों ने तमाम परिषदों में से एक तिहाई जीत हासिल की, पूंजीपति वर्ग के लिए खतरे का संकेत था, जिन्होंने तुरंत एक ऐसी ताकत की तलाश शुरू कर दी जो क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग का मुकाबला कर सके। यह वही समय था जब मुसोलिनी के फाशीस्मो (fascismo) को कुछ महत्व प्राप्त हुआ था। फ़ैक्टरियों पर कब्जे में सर्वहारा वर्ग की हार के बाद फासीवादियों (fascisti) की संख्या 1,000 से अधिक हो गई और उसका एक बड़ा हिस्सा मुसोलिनी के संगठन में शामिल हो गया। दूसरी ओर, सर्वहारा वर्ग का विशाल जनसमूह उदासीनता की चपेट में आ गया था। फासिस्टों की पहली सफलता का कारण यह था कि उन्होंने अपनी शुरुआत क्रांतिकारी हावभाव से की थी। उनका दिखावटी उद्देश्य क्रांतिकारी युद्ध की क्रांतिकारी विजय को बरकरार रखने के लिए लड़ना था, और इस कारण से उन्होंने एक मजबूत राज्य की मांग की जो समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिरोधी हितों के खिलाफ, जिनका प्रतिनिधित्व “पुराना राज्य” करता था, जीत के इन क्रांतिकारी फलों की रक्षा करने में सक्षम होगा। इनका नारा सभी शोषकों के खिलाफ था, और इसलिए पूंजीपति वर्ग के खिलाफ भी था। उस समय फासीवाद इतना कट्टरपंथी था कि उसने जियोलित्ती को फांसी देने और इतालवी राजवंश को गद्दी से हटाने की भी मांग की। लेकिन जियोलित्ती ने सावधानीपूर्वक फासीवाद, जिसे वह कम बुरा मानता था, के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने से परहेज किया। इन फासीवादी दावों को संतुष्ट करने के लिए उसने संसद को भंग कर दिया। उस समय मुसोलिनी अभी भी रिपब्लिकन होने का दिखावा कर रहा था, और एक साक्षात्कार में उसने घोषणा की कि फासीवादी गुट इतालवी संसद के उद्घाटन में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह राजशाही समारोह के साथ होना था। इन कथनों ने फासीवादी आंदोलन में संकट पैदा कर दिया, जिसे मुसोलिनी के अनुयायियों और राजशाही संगठन के प्रतिनिधियों के विलय के बाद पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था, और नई पार्टी की कार्यकारिणी दोनों गुटों के बराबर प्रतिनिधित्व से बनी थी। फासीवादी पार्टी ने मजदूर वर्ग को भ्रष्ट और आतंकित करने का दोधारी हथियार निर्मित किया। श्रमिक वर्ग को भ्रष्ट करने के लिए फासीवादी ट्रेड यूनियनें, तथाकथित निगम जिनमें श्रमिक और नियोक्ता एकजुट थे, बनाई गईं। मजदूर वर्ग को आतंकित करने के लिए फासीवादी पार्टी ने उग्रवादी दस्ते बनाए जो दंड देने के अभियानों से विकसित हुए थे। यहां इस बात पर फिर से जोर दिया जाना चाहिए कि आम हड़ताल के दौरान इतालवी सुधारवादियों की जबरदस्त दगाबाजी, जो इतालवी सर्वहारा वर्ग की भयानक हार का कारण बनी, ने फासीवादियों को राजसत्ता पर कब्जा करने के लिए सीधा प्रोत्साहन दिया था। दूसरी ओर, कम्युनिस्ट पार्टी की गलतियों का आधार फासीवाद को बिना किसी गहन सामाजिक आधार के महज एक सैन्यवादी और आतंकवादी आंदोलन मानना था।
आइए अब देखें कि फासीवाद ने सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद से अपने इच्छित क्रांतिकारी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, वर्ग रहित राज्य बनाने के अपने वादे को साकार करने के लिए क्या किया है। फासीवाद ने एक नए और बेहतर चुनावी कानून और महिलाओं के लिए समान मताधिकार का वादा किया। मुसोलिनी का नया मताधिकार कानून वास्तव में फासीवादी आंदोलन के पक्ष में मताधिकार कानून का निकृष्टतम अवरोधक है। इस कानून के अनुसार, सभी सीटों में से दो-तिहाई सीटें सबसे मजबूत पार्टी को दी जानी चाहिए, और अन्य सभी दलों के पास कुल मिलाकर केवल एक-तिहाई सीटें होंगी। महिलाओं का मताधिकार लगभग पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। वोट देने का अधिकार केवल धनी महिलाओं और तथाकथित “युद्ध-प्रतिष्ठित” महिलाओं के एक छोटे समूह को दिया गया है। आर्थिक संसद और नेशनल असेंबली के वादे का अब कोई उल्लेख नहीं होता है, न ही सीनेट के उन्मूलन का, जिसकी फासीवादियों ने इतनी गंभीरता से प्रतिज्ञा की थी।
सामाजिक क्षेत्र में की गई संकल्पों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। फासिस्टों ने अपने कार्यक्रम में आठ-घंटे कार्यदिवस की घोषणा की थी, लेकिन उनके द्वारा पेश किये गये विधेयक में इतने सारे अपवादों का प्रावधान है कि इटली में आठ घंटे कार्यदिवस नहीं होना तय है। मजदूरी की गारंटी के वादे का भी कुछ नहीं हुआ। ट्रेड यूनियनों के विनाश ने नियोक्ताओं को 20 से 30 प्रतिशत और कुछ मामलों में 50 से 60 प्रतिशत तक वेतन कटौती करने का अधिकार दे दिया है। फासीवाद ने वृद्धावस्था और विकलांग बीमा का वादा किया था। व्यवहार में, फासीवादी सरकार ने, अर्थव्यवस्था की खातिर, बजट में इस उद्देश्य के लिए अलग रखे गए 50,000,000 लीरे की तुच्छ राशि को भी हटा दिया है। श्रमिकों को कारखानों के प्रशासन में तकनीकी भागीदारी के अधिकार का वादा किया गया था। आज इटली में एक कानून है जो फ़ैक्टरी कौंसिलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। राजकीय उद्यम निजी पूंजी के हाथों में खेल रहे हैं। फासीवादी कार्यक्रम में पूंजी पर प्रगतिशील आयकर का प्रावधान था, जो कुछ हद तक पूंजीवादी स्वामित्व को कमजोर करने का काम करता। वास्तव में जो हुआ वह लेकिन इसके विपरीत था। विलासिता की वस्तुओं पर विभिन्न करों को, जैसे ऑटोमोबाइल कर, समाप्त कर दिया गया, दलील दी गई कि यह राष्ट्रीय उत्पादन को अवरुद्ध करेगा। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि इस कारण से की गई थी कि इससे घरेलू खपत में कमी आएगी और इस प्रकार निर्यात की संभावनाओं में सुधार होगा। फासीवादी सरकार ने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (transfer of securities) के अनिवार्य पंजीकरण के कानून को भी निरस्त कर दिया, इस प्रकार बियरर-बांड की प्रणाली को फिर से शुरू किया और कर चोरी करने वालों के लिए दरवाजा खोल दिया। स्कूलों को पादरी वर्ग को सौंप दिया गया। राजसत्ता पर कब्जा करने से पहले, मुसोलिनी ने एक आयोग की मांग की थी जो युद्ध से हुए मुनाफे (war profits) की जांच करेगा और उसमें से 85 प्रतिशत राज्य को सौंप दिया जाएगा। जब यह आयोग मुसोलिनी के वित्तीय सरपरस्तों, भारी उद्योगपतियों के लिए असहज हो गया, तो उसने आदेश दिया कि आयोग केवल उसे ही रिपोर्ट सौंपे, और जो कोई भी उस आयोग में घटित कोई भी बात को प्रकाशित करेगा, उसे छह महीने की कैद की सजा दी जाएगी। सैन्य मामलों में भी फासीवाद अपने वादे निभाने में विफल रहा। सेना को क्षेत्रीय रक्षा तक सीमित रखने का वादा किया गया था। वास्तव में, स्थायी सेना के लिए सेवा की अवधि आठ महीने से बढ़ाकर अठारह कर दी गई, जिसका मतलब था कि सशस्त्र बलों की संख्या 250,000 से बढ़कर 350,000 हो गई। रॉयल गार्ड्स को समाप्त कर दिया गया क्योंकि वे मुसोलिनी के लिए बहुत लोकतांत्रिक थे। दूसरी ओर, काराबेनियरी (अर्धसैनिक पुलिस फोर्स) को 65,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया और सभी पुलिस टुकड़ियों को दोगुना कर दिया गया। फासीवादी संगठन राष्ट्रीय मिलिशिया के रूप में तब्दील हो गए, जिनकी संख्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अब 500,000 तक पहुंच गई है। लेकिन सामाजिक मतभेदों ने मिलिशिया में राजनीतिक विरोधाभास का बीज बो दिया है, जो अंततः फासीवाद के पतन का कारण बनेगा।
जब हम फासीवादी कार्यक्रम की तुलना उसके पालन से करते हैं तो हम आज ही इटली में फासीवाद के पूर्ण वैचारिक पतन का अनुमान लगा सकते हैं। इस वैचारिक दिवालियेपन के बाद राजनीतिक दिवालियापन अनिवार्य रूप से सामने आता है। फासीवाद उन ताकतों को एक साथ रखने में असमर्थ है जिन्होंने उसे सत्ता में आने में मदद की। कई रूपों में हितों का टकराव पहले से ही महसूस किया जा रहा है। फासीवाद पुरानी नौकरशाही को अपने अधीन बनाने में अभी तक सफल नहीं हुआ है। सेना में पुराने अधिकारियों और नये फासीवादी नेताओं के बीच भी मनमुटाव है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में फासीवाद के ख़िलाफ़ प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। वर्ग विरोध फासिस्टों की कतारों में भी व्याप्त होना शुरू हो गया है। फासीवादी उन वादों को पूरा करने में असमर्थ हैं जो उन्होंने श्रमिकों और फासीवादी ट्रेड यूनियनों से किये थे। मज़दूरों की मज़दूरी में कटौती और बर्खास्तगी आजकल आम बात हो गई है। इसीलिए फासीवादी ट्रेड यूनियन आंदोलन के खिलाफ पहला विरोध स्वयं फासीवादियों की कतार से आया था। मजदूर शीघ्र ही अपने वर्गीय हित एवं वर्गीय दायित्व पर वापस आयेंगे। हमें फासीवाद को एकजुट शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए जो हमारे हमले को विफल करने में सक्षम हो। बल्कि वह ऐसा गठन है, जिसमें कई विरोधी तत्व शामिल हैं, और वह भीतर से विघटित हो जाएगा। लेकिन यह मानना खतरनाक होगा कि इटली में फासीवाद के वैचारिक और राजनीतिक विघटन के तुरंत बाद सैन्य विघटन होगा। इसके विपरीत, आतंकवादी तरीकों से फासीवाद द्वारा जीवित रहने के प्रयास के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए, क्रांतिकारी इतालवी श्रमिकों को आगे के गंभीर संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम विघटन की इस प्रक्रिया के महज दर्शक बन संतुष्ट रहे तो यह बहुत बड़ी विपत्ति होगी। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उपलब्ध सभी साधनों के साथ इस प्रक्रिया को तेज करें। यह न केवल इतालवी सर्वहारा वर्ग का कर्तव्य है, बल्कि जर्मन फासीवाद के सामने जर्मन सर्वहारा वर्ग का भी कर्तव्य है।
इटली के बाद जर्मनी में फासीवाद सबसे मजबूत है। युद्ध के परिणाम और क्रांति की विफलता के नतीजतन, जर्मनी की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कमजोर है, और किसी अन्य देश में क्रांति के लिए वस्तुनिष्ठ परिपक्वता और श्रमिक वर्ग की आत्मपरक तैयारी के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं है जितना कि अभी जर्मनी में। किसी भी अन्य देश में सुधारवादी इतनी बुरी तरह असफल नहीं हुए जितना कि जर्मनी में। उनकी विफलता पुराने इंटरनेशनल में किसी भी अन्य पार्टी की विफलता से अधिक आपराधिक है, क्योंकि उन्हें ही उस देश में, जहां मजदूर वर्ग के संगठन पुराने और अन्यत्र की तुलना में बेहतर व्यवस्थित हैं, सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए बिल्कुल अलग तरीकों से संघर्ष करना चाहिए था।
मुझे पूरा यकीन है कि न तो शांति संधियों और न ही रूर (Ruhr) के कब्जे से जर्मनी में फासीवाद को वैसा बढ़ावा मिला है जितना कि मुसोलिनी द्वारा सत्ता हथियाने से । इससे जर्मन फासिस्ट प्रोत्साहित हुए हैं। इटली में फासीवाद का खात्मा जर्मनी में फासीवादियों का हौसला पस्त करेगा । हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए: विदेशों में फासीवाद को उखाड़ फेंकने की शर्त हर एक देश में इन देशों के सर्वहारा द्वारा फासीवाद को उखाड़ फेंकना है। हमारा दायित्व है कि हम वैचारिक और राजनीतिक रूप से फासीवाद पर विजय प्राप्त करें। यह हम पर भारी कार्यभार थोपता है। हमें समझना होगा कि फासीवाद निराश लोगों का और उन लोगों का आंदोलन है जिनका अस्तित्व नष्ट हो गया है। इसलिए, हमें उस व्यापक जनसमूह को जीतने या बेअसर करने का प्रयास करना चाहिए जो अभी भी फासीवादी खेमे में हैं। मैं अपने इस एहसास के महत्व पर जोर देना चाहती हूं कि हमें इस जनता की आत्मा पर कब्ज़ा करने के लिए वैचारिक रूप से संघर्ष करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि वे न केवल अपने वर्तमान कष्टों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वे एक नए दर्शन के लिए लालायित हैं। हमें अपनी वर्तमान गतिविधि की संकीर्ण सीमाओं से बाहर आना होगा। तीसरा इंटरनेशनल, पुराने इंटरनेशनल के विपरीत, बिना किसी भेदभाव के सभी नस्लों का इंटरनेशनल है। कम्युनिस्ट पार्टियों को न केवल शारीरिक सर्वहारा श्रमिकों का अगुआ होना चाहिए, बल्कि दिमागी श्रमिकों के हितों का ऊर्जावान रक्षक भी होना चाहिए। उन्हें समाज के उन सभी वर्गों का नेता होना चाहिए जो अपने हितों और भविष्य की अपेक्षाओं के कारण बुर्जुआ वर्चस्व के विरोध में हैं। इसलिए, मैंने (इस साल जून में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की विस्तारित कार्यकारी समिति के एक सत्र में बोलते हुए) मजदूरों और किसानों की सरकार के लिए संघर्ष शुरू करने के लिए कॉमरेड ज़िनोविएव के प्रस्ताव का स्वागत किया। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुई। यह नया नारा सभी देशों के लिए बहुत मायने रखता है। फासीवाद को उखाड़ फेंकने के संघर्ष में हम इससे दूर नहीं रह सकते। इसका अर्थ है कि छोटे किसानों की व्यापक जनता का उद्धार साम्यवाद के माध्यम से होगा। हमें अपने आप को केवल अपने राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम के लिए संघर्ष करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें साथ ही एक दर्शन के रूप में साम्यवाद के आदर्शों से जनता को परिचित कराना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम उन सभी तत्वों को एक नए दर्शन का मार्ग दिखाएंगे, जिन्होंने हाल के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में अपना असर खो दिया है। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि, जैसे-जैसे हम इन जनता के पास पहुंचते हैं, हम संगठनात्मक रूप से, एक पार्टी के रूप में, एक मजबूती से जुड़ी हुई इकाई बन जाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अवसरवादिता में फंसने और दिवालिया हो जाने का जोखिम उठाते हैं। हमें अपने काम के तरीकों को अपने नये कार्यों के अनुरूप ढालना होगा। हमें जनता से ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसे वो, हमारे विचारों पर पूर्वाग्रह के बिना, समझ सके। इस प्रकार, फासीवाद के खिलाफ संघर्ष कई नए कार्यभारों को सामने लाता है।
यह सभी पार्टियों का दायित्व है कि वे इस कार्यभार को ऊर्जावान ढंग से और अपने-अपने देश की स्थिति के अनुरूप पूरा करें। हालाँकि, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वैचारिक और राजनीतिक रूप से फासीवाद पर काबू पाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। फासीवाद से उसके मुकाबले में सर्वहारा वर्ग की स्थिति वर्तमान में आत्मरक्षा की है। सर्वहारा वर्ग की इस आत्मरक्षा को उसके अस्तित्व और उसके संगठन के लिए संघर्ष का रूप लेना होगा।
सर्वहारा वर्ग के पास आत्मरक्षा का सुव्यवस्थित तंत्र होना चाहिए। जब भी फासीवाद हिंसा का प्रयोग करता है, तो उसका सामना सर्वहारा हिंसा से ही करना पड़ता है। मेरा तात्पर्य व्यक्तिगत आतंकवादी कृत्यों से नहीं, बल्कि सर्वहारा वर्ग के संगठित क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष की हिंसा से है। जर्मनी ने “सर्वहारा सौ” (proletarische hundertschaften — श्रमिक मिलिशिया) संगठित करके एक शुरुआत की है। यह संघर्ष तभी सफल हो सकता है जब सर्वहारा संयुक्त मोर्चा हो। श्रमिकों को पार्टी से ऊपर उठकर इस संघर्ष के लिए एकजुट होना होगा। सर्वहारा वर्ग की आत्मरक्षा सर्वहारा संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए सबसे बड़े प्रोत्साहनों में से एक है। प्रत्येक श्रमिक की आत्मा में वर्ग-चेतना पैदा करके ही हम फासीवाद को सैन्य रूप से उखाड़ फेंकने के लिए भी तैयारी करने में सफल होंगे, जो इस समय नितांत आवश्यक है। यदि हम इसमें सफल होते हैं, तो हम यकीन कर सकते हैं कि सर्वहारा वर्ग के खिलाफ पूंजीपति वर्ग के आम आक्रमण की सफलताओं के बावजूद, जल्द ही पूंजीवादी व्यवस्था और बुर्जुआ शक्ति का काम तमाम हो जाएगा। विघटन के चिन्ह, जो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि महाकाय सर्वहारा फिर से क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल होगा, और तब पूंजीवादी दुनिया के लिए उसका आह्वान होगा: मैं शक्ति हूं, मैं संकल्प हूं, मुझमें तुम भविष्य देखते हो!