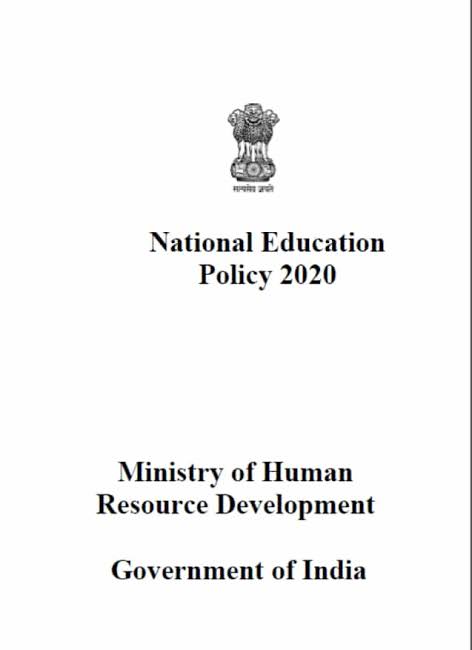संपादकीय, मोर्चा पत्रिका (draft)
2022 में इटली में जियोर्जिया मेलोनी की जीत ने चरम-दक्षिणपंथियों में आत्म-विश्वास भर दिया था। आज छह यूरोपीय संघ के देश — इटली, फ़िनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक गणराज्य — में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं। स्वीडन में वे संसदीय ताकत के आधार पर दूसरे नंबर पर हैं, नीदरलैंड की संसद में गीर्ट विल्डर्स की चरम दक्षिणपंथी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और सरकार बनाने के कगार पर है। इस साल जून के महीने में हुए यूरोपीय संघ के चुनाव में पूरे यूरोप में दक्षिणपंथियों को अपार सफलता मिली है – तमाम संघीय देशों में दक्षिणपंथ की राजनीतिक पैठ मजबूत हुई है। इस चुनाव में शिकस्त के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हड़बड़ी में संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी जिसमें पहली बार दक्षिणपंथी मारी ले पेन की पार्टी सर्वाधिक जनप्रिय पार्टी के रूप में उभरी है। यह बात अलग है कि गैर–दक्षिणपंथियों के विभिन्न पार्टियों ने चुनाव के दूसरे दौर में आपसी व्यावहारिक गठजोड़ द्वारा ले पेन की पार्टी को सीट के आधार पर तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। इस तरह के पराजय की कुंठा उसकी राजनीति और व्यापक यूरोपीय समाज पर क्या असर करेगी, यह समय के साथ ही पता चलेगा। इसके अलावे नाइजेल फ़राज़ की पार्टी, रिफॉर्म यूके ने इस बार ब्रिटेन के चुनाव में पांच सीट जीता है और कुल मिलाकर 15 प्रतिशत वोट प्राप्त किया है, जोकि अभूतपूर्व है। 2019 में उसे बस 2 प्रतिशत वोट मिले थे।
हमारा मानना है कि फासीवादी और कट्टर दक्षिणपंथ की राजनीति के इस फैलाव को महज उसके अपने औपचारिक व्याकरण के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उसके कुत्सित कारनामों का अवश्य ही विरोध होना चाहिए और फौरी तौर पर उसका प्रतिकार होना चाहिए, परंतु उस राजनीति की या कहें किसी भी राजनीति और राजनीतिक विचारधारा की सामाजिक प्रक्रियाओं से अलहदा अपनी गति नहीं होती। इन्हीं सामाजिक प्रक्रियाओं और उनमें अंतर्निहित अंतर्विरोधों, विकल्पों तथा संभावनाओं का उच्चारण ये राजनीतिक विचारधाराएं और गतिविधियां करती हैं। शायद इसी अर्थ में मार्क्स ने राजनीति, विधि, विज्ञान, कला, मजहब इत्यादि के इतिहास न होने की बात कही थी। इनका अपना इतिहास नहीं होता। फासीवाद अथवा कट्टर–दक्षिणपंथ का आंतरिक इतिहास लिखने वाले वंशावली विशेषज्ञ या फिर गोत्र का इतिहास लिखने वाले पंडों के प्रतिरूप हैं, जिनके लिए पाणिनी के “अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्” में ही पूरा इतिहास सूत्रबद्ध है। “इतिहास की अब तक की मान्य अवधारणा कितनी हास्यास्पद है जो वास्तविक संबंधों की उपेक्षा करती है तथा अपने को राजाओं तथा राज्यों के आडंबरपूर्ण नाटकों तक सीमित रखती है।” – मार्क्स की यह बात आज भी अधिकांश राजनीतिक व्याख्याकारों और इतिहासकारों पर लागू होती है। बस आज उन राजाओं की जगह नामित पार्टियों, नेताओं और संसदीय अखाड़े में उनकी नौटंकियों ने ले ली है।
नाज़ी–फासीवादी प्रचार के जन–आकर्षण की नींव 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में यूरोपीय स्तर पर सामाजिक क्रांति के फैलाव की संभावनाओं पर भितरघाती और राजकीय दमन के नतीजे में दिखती है। प्रथम विश्वयुद्ध से बदहाल श्रमिक जनता, बेरोजगारी, गरीबी और पूंजीवादी संचय के विनाशकारी नतीजों के खिलाफ सोवियत व वर्कर्स कौंसिल जैसे समाजवादी अनुभवों में सामाजिक-आर्थिक संबंधों को पुनर्नियोजित कर पूंजीवादी अलगाव को मिटाकर श्रम-जीवन पर स्व-नियंत्रण (तमिल कम्युनिस्ट मलयपुरम सिंगरावेलु चेट्टियार की भाषा में “श्रम स्वराज”) की संभावना को देख रहे थे। परंतु मजदूर आंदोलन में निम्न–पूंजीवादी राजकीयवादी नेतृत्व ने राजसत्ता की प्रबंधक प्रणाली के अंग बनकर इन अनुभवों के क्रांतिकारी सामान्यीकरण (revolutionary generalisation) की गुंजाइश को नष्ट कर दिया। रोज़ा लुक्सेम्बुर्ग और कार्ल लिबनेख्त जैसे विख्यात क्रांतिकारियों और मार्क्सवादी विचारकों की हत्या इस दौर में हुई।
फासीवाद यूरोप में क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन की राख पर पनपा था। सोवियत क्रांति ने विश्वभर में शोषित जनता के अंदर जिस उम्मीद को जगाई थी, उसके दमन ने फासीवादी दक्षिणपंथ को जन्म दिया। जैसा कि जर्मनी की महान क्रांतिकारी नेता क्लारा जेटकिन ने कहा था, “फासीवाद, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सर्वहारा आक्रामकता के प्रतिशोध में पूंजीपति वर्ग का बदला नहीं है, बल्कि वह रूस में शुरू हुई क्रांति को जारी रखने में विफल रहने के लिए सर्वहारा वर्ग की सजा है।” इटली के कम्युनिस्ट विचारक अंतोनियो ग्राम्शी ने इसी बात को और गहनता से रखा – “संकट इस तथ्य में निहित है कि पुराना मर रहा है और नये का जन्म नहीं हो सकता; इस अंतराल में विभिन्न प्रकार के रुग्ण लक्षण प्रकट होते हैं।” सामाजिक क्रांति के दमन ने जिन रुग्ण लक्षणों को जन्म दिया उनका ही एकीकृत रूप फासीवाद था। कम्युनिस्ट इंटरनैशनल के नेता ज्यॉर्जी दिमित्रोव ने साफ शब्दों में फासीवाद के आकर्षण के स्रोतों की तरफ इंगित किया था। उनके अनुसार वह आम जनता की “सबसे फौरी जरूरतों और मांगों को लफ्फाजी के साथ पेश करता है। वह न सिर्फ आम जनता में गहरे पैठे हुए पूर्वाग्रहों को प्रज्वलित करता है, बल्कि आम जनता की उदात्त भावनाओं को, उनके न्याय-बोध को, और कभी-कभी तो उनकी क्रांतिकारी परंपराओं को भी, उकसाता है।” वह अपने आपको “अन्याय के शिकार राष्ट्र के हित-रक्षक” के रूप में पेश कर “आहत राष्ट्रीय भावनाओं को सहलाता है”।”
राजनीतिक आर्थिक संकटों से जूझते पूंजीवाद को अपने आप को बनाए रखने के लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत होती है। फासीवाद सामाजिक क्रांति की ऊर्जा के विस्थापन और उसकी राष्ट्रवादी घनीभूति के रूप में 20वीं सदी में पूंजीवादी पुनरुत्थान के लिए अवसर तैयार करने में कारगर रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1929 के मंदी के नतीजतन पूंजीवादी ह्रास से निजाद पाने के लिए फासीवाद ने नई राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विकसित करने का अवसर प्रदान किया। यही संस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी विस्तार को पुनर्नियोजित करने की आधारभूत संरचना बनी। प्रतिस्पर्धात्मक सैन्यीकरण और सैन्य-औद्योगिक परिसरों के प्रसार द्वारा वैश्विक पूंजीवादी संचय की प्रक्रिया को बनाए रखने की सीख फासीवाद ने ही दी (दानिएल गेरीं और फ्रांज़ नोएमन्न के प्रतिष्ठित कामों को देखें)।
आज पूंजीवाद के नवोदारवादी दौर में, वित्तीयकरण और पूँजी परिपथ के भूमंडलीकरण ने अर्थतंत्र की नीति-आधारित राजकीय प्रबन्धन व्यवस्था को लगभग निरस्त कर दिया है, जिसके कारण मांग-आधारित संघर्षों की पुरानी संस्थाओं का असर कमजोर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बढ़ती अनिश्चितताओं, अलगाव और अति-प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त सर्वहाराकृत, बेशीकृत और दरिद्रीकृत “व्यक्तियों” की भीड़, चरम-दक्षिणपंथी राजनीति का स्वाभाविक ग्राहक बन जाती है। राजसत्ता का काम महज इस भीड़ को पूंजीवादी यथास्थिति के हित में प्रबंधित करना है, उसके अंदर विद्यमान वर्गीय आत्म-मुक्ति की प्रच्छन्न प्रक्रियाओं और संभावनाओं को खंडित कर कुंद करना है। यही नवक्लासिकीय अर्थशास्त्र और नवोदारवाद के तहत राजसत्ता का न्यूनतमीकरण (minimisation of the state) है। और इसी अर्थ में चरम दक्षिणपंथ का सतत योगदान होता है। आज विश्व भर में चरम–दक्षिणपंथी राजनीति का फैलाव दिखाता है कि पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था वैश्विक स्तर पर संकट में है। चरम–दक्षिणपंथ संकट का लक्षण है और साथ ही वह संकटग्रस्त निवारण है।
यूरोप में आज जो सोच समूचे दक्षिणपंथ को (उसके रूढ़िवादी, चरम और फासीवादी रूपों को) परिभाषित करती है और एक साथ लाती है, वह है उनका तीव्र अति-राष्ट्रवादी, नस्लवादी प्रवासी-विरोध, जिसने पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजसत्ता की उदारवादी नींव को खतरे में डाल दिया है — नागरिकता के अधिकार को इनकी राजनीति लगातार विशेषाधिकार के रूप में पेश करती रही है। यह प्रवासी-विरोध विश्व पूंजीवाद के खिलाफ विरोध को कमजोर करता है। और यही बात इस राजनीति को पूंजीवाद के संकट के दौर में आकर्षक बनाती है।
परंतु भारत के चुनाव में क्या हुआ? बात सही है कि मोदी कमजोर पड़े मगर हारे नहीं। लेकिन जब विश्व में हर जगह चरम दक्षिणपंथ की साख बढ़ रही है, तो विश्वगुरु की यह गति क्यों? क्या हुआ कि आरएसएस के प्रचारक राम माधव जो 28 अप्रैल को “भारत को वैश्विक रूढ़िवादी आंदोलन का नेतृत्व” करने की बात कह रहे थे, वो अब (13 जुलाई को) बहुवाद और भिन्नता का आदर करते हुए भारतीय और पाश्चात्य रूढ़िवादियों के बीच सहयोग ढूंढ रहे हैं? कहाँ गई विश्वगुरु की हेकड़ी?
भारतीय चुनाव – बदले–बदले मेरे सरकार नजर आते हैं!
भारत के 2024 के चुनावी नतीजे ने चुनावोत्तर संसदीय राजनीति को शायद रोचक बना दिया है। मोदी के नेतृत्व में सरकार फिर से गठित हो गई है, मगर कमजोर बहुमत के साथ। दूसरी तरफ विपक्ष की जमीन थोड़ी फैली है, और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें राजनीतिक पहचान मिल गई है। परंतु बदला क्या है? ज्यादातर गंभीर व्याख्याकारों का मानना है कि सरकार के काम के तरीके और तेवर में कोई खास बदलाव नहीं होगा – बल्कि भाजपा नेताओं के प्रतिहिंसक रवैये में बढ़ोत्तरी हो सकती है। चुनाव के बाद के पहले संसदीय सत्र में ऐसा ही देखने को मिला – एक तरफ अगर विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ा है, तो दूसरी तरफ भाजपाइयों की कुंठित प्रवृत्ति ने तीव्र रूप लिया है। कुछ भाजपा सांसदों ने तो अपनी कुंठा अपने इलाके के मतदाताओं पर निकालनी शुरू कर दी है। जिस रूप में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद (जहां अयोध्या है) की जनता को हिन्दू-विरोधी रामद्रोही कहा जा रहा है वह भी यही दर्शाता है। बीजेपी के बंगाल के नेता शुभेन्दु अधिकारी ने तो मोदी के “सबका साथ सबका विकास” के नारे को तिलांजलि देकर “जो हमारे साथ, हम उनके साथ” का नारा लगाने की बात कही है। आर्थिक नीति के क्षेत्र में, सीपी चंद्रशेखर (24 जून फ्रंटलाईन) के अनुसार , “हालाँकि आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए नई सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन दीर्घस्थायी राजनीतिक उद्देश्य महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों में बाधा बन सकते हैं।”
कई व्याख्याकार इस बार के चुनावी नतीजे को राष्ट्रीय पटल पर क्षेत्रीय शक्तियों और गठबंधन राजनीति के पुनरागमन के रूप में देखते हैं। पिछले एक दशक से चल रहे सत्ता के केंद्रीकरण पर इस चुनाव ने रोक लगा दिया है। यह सच है कि मोदी सरकार इस बार एनडीए के अन्य घटकों पर निर्भर है, और विपक्ष की मजबूती भी कांग्रेस के साथ बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के आपसी तालमेल पर निर्भर है। अवश्य ही क्षेत्रीय दलों के महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखना होगा, परंतु सत्ता केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से ये क्षेत्रीय दल भी अछूते नहीं हैं। बंगाल की ममता सरकार या आंध्रप्रदेश में नायडू सरकार का इतिहास निरंकुशता और केंद्रीकरण के मामले में भाजपा से कम नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार के निरंकुश व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए दलीय दांवपेच नाकाफी होगी। बैसाखी का इस्तेमाल डंडे के रूप में भी हो सकता है अथवा उसके अंदर भाले भी छुपे हो सकते हैं। या फिर किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने वाली बात भी हो सकती है।
जहां तक भाजपा/आरएसएस के एजेंडे का सवाल है, वह किसी न किसी रूप में सामने आएगा, सरकारी स्तर पर जो ढीला प्रतीत होगा उसे सांगठनिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश होगी। इस चुनाव के नतीजे के बाद, सरकार द्वारा ऊपर से थोपे हुए एजेंडे से बेहतर है नीचे से सर्वसम्मति पैदा की जाए, जिसके लिए आरएसएस के सांगठनिक नेटवर्क से अच्छा कुछ नही है। कुछ लोग आरएसएस प्रमुख और अन्य प्रभारियों के बयानों में मोदी और संघ के बीच फासले को देख रहे हैं – जिसमें मोदी की तुलना में संघ ज्यादा नैतिक प्रतीत होता है। इस तरह के बयान और उन पर व्याख्याएं संघी विचारधारा को सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर पर सामान्य बनाने का काम करती हैं। इस तरह के कथित और कल्पित फासले की अफवाह संघ द्वारा अपने लिए जगह बनाने में काम करते हैं, जो संसदीय राजनीतिक दायरे में भाजपा को ही मजबूत करेगा।
जो सीटों के आधार पर दक्षिणपंथ की सामाजिक राजनीतिक पकड़ को आँकते हैं उन्हें इस बार के चुनावी आंकड़ों को ध्यान से देखना चाहिए। योगेंद्र यादव और उनके साथियों के अनुसार (द प्रिन्ट, 11 जून) बीजेपी के वोट प्रतिशत में मामूली गिरावट आई है — ओडिशा में ऐतिहासिक जीत के साथ-साथ, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र में उसने बढ़िया प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने देश के हर राज्य में दोहरे अंकों के वोट प्रतिशत पाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निर्विवाद उपस्थिति दर्ज की है। वे यह भी कहते हैं कि इस बार दो विभिन्न बीजेपी चुनावी मैदान में थे — शासक बीजेपी और दावेदार बीजेपी। उनके अनुसार शासक बीजेपी को गंभीर चुनावी उलटफेर का सामना करना पड़ा, जबकि दावेदार बीजेपी का चुनावी प्रदर्शन बढ़िया रहा। इसका स्वाभाविक अर्थ है कि इस चुनाव को दावेदारों ने जीता है — यानि इस बार का चुनाव परिणाम अधिकांशतः यथास्थिति के खिलाफ था — उसका निषेधात्मक चरित्र था। संसदीय चुनाव के सीमित दायरे में सत्ता को इसी तरह से ठुकराया जा सकता है। ब्लूमबर्ग (जून 5) के पत्रकारों के अनुसार — “मोदी के समर्थन का पतन [विशेषकर उत्तर प्रदेश में], दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में पीछे रह गए लाखों लोगों के सामूहिक विद्रोह के समान था।”
हाल के दशकों में भारत में उम्मीद के आधार पर शायद ही चुनाव जीते गए हैं। जनता ने किसी प्रकार की राजनीति पर विश्वास कर के उन्हें नहीं चुना है, उसने हर चुनाव में अपनी तंगी को महसूस कर, सरकारों और पार्टियों को सबक सिखाने का काम किया है। “दावेदारों” को जो फायदा हो रहा है, वह अंततः उनकी मेहनत या जनता का उनपर विश्वास से ज्यादा, जनता की आम उदासीनता और गुस्से का नतीजा है। 2014 के गणतंत्र दिवस की पूर्व-संध्या पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में इस गुस्से की ओर साफ इंगित किया था — राजनीतिज्ञों द्वारा लोकतंत्र में निहित “पवित्र भरोसे” (sacred trust) के तोड़े जाने के कारण “सड़क से हताशा के स्वर” सुनाई दे रहे हैं। इस पवित्र भरोसे के टूटने से मोहभंग होता है, “जिससे क्रोध भड़कता है तथा इस क्रोध का एक ही स्वाभाविक निशाना होता है : सत्ताधारी वर्ग।” 2014 में मोदी सरकार के गठन में इसी क्रोध का योगदान था। नवोदारवादी दौर में पूंजीवादी राजसत्ता के लिए एक ही काम तय है — कि इस गुस्से की ऊर्जा को वह पूँजी के हित में उत्पादक बनाए। अंधा राष्ट्रवाद, धार्मिक उन्माद और मोदी-शाह का दबंग मनमानापन कुछ हद तक इस गुस्से को बांधने में कारगर होते हैं, परंतु संकट गहरा है — राजसत्ता के पास भरोसा पैदा करने के हथकंडे कम होते जा रहे हैं। पहचानों के आधार पर भारत की (अल्परोजगारी और बेरोजगारी से ग्रस्त) मेहनतकश जनता को लामबंध कर विभाजित और प्रतिस्पर्धा में रखने की सीमा है — वर्गीय प्रक्रियाएं भूमिगत ही सही ऐन मौकों पर रंग दिखला ही देती हैं। मोदी ने चुनाव के दौरान धनाढ्य मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग की बेचैनी को धन-पुनर्वितरण के सवाल पर जिस रूप से आम जनता पर थोपना चाहा, वह राजसत्ता के वर्गीय चरित्र को पूरी तरह से नंगा करता है। सामूहिक विद्रोह जो हम लगातार देख रहे हैं, उसने सत्ताधारी शक्तियों और उनके पोशक वर्गों को बेचैन कर दिया है — चाहे कोविड महामारी के दौरान लाखों मजदूरों की घर वापसी हो, जो कि भारतीय राजतंत्र की अमानवीय निरंकुशता केखिलाफ खामोश बगावत थी, या फिर 2020-21 का किसान आंदोलन जिसने मोदी सरकार के मानमानेपन की धज्जियाँ उड़ा दीं। इस प्रकार की सामूहिकता शासन व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती है, और यही दक्षिणपंथ पर भी लगाम लगाने का काम करती है। हम आज फ्रांस में भी यही देख रहे हैं ।
सामूहिकता सत्ता के गलियारे की दासी नहीं है, वह निर्बाध गंगा है — वही है जो सत्ता को पैदा करती है और अपने मौज में उसे बहा देती है। सामूहिकता से सत्ता पैदा होती है और जब बेलगाम हो सत्ता उसी के सिर पर नाचने लगती है तो फिर एक बार विद्रोह की आग की जरूरत होती है उसे भस्म करने के लिए। भारत में नवोदारवादी पूंजीवाद की आधार-संरचना के विकास में सभी राजनीतिक पार्टियों का योगदान रहा — जो उसके लक्षणों और प्रभावों का विरोध भी करते रहे, वे सत्तासीन हो या सत्ता के करीब हो या फिर उसके साथ वार्तालीन हो, नवोदारवादी प्रक्रिया के साधन बन गए। संसदीय और राजकीयवादी राजनीति द्वारा वित्तीयकृत और सूचनाकृत पूँजी पर लगाम लगाने की सोच रखने वाले कीन्सवादी राजकीयवादी विरह (nostalgia) के शिकार हैं। विश्व के अधिकांश संसदीय वामपंथ इसी विषाद में जीते हैं और सत्ता के संघर्ष में उनकी दुर्गति ही होती है — लातिन अमरीका के कई देशों के, यूनान में सीरीज़ा के अनुभव इसी ओर इंगित करते हैं। जो सामूहिक विद्रोह उन्हें सत्तासीन करती है, अंततः उसी विद्रोह को उन्हें नियंत्रित करना होता है — और यही आधार बनता है चरम-दक्षिणपंथ के फैलाव का — ब्राजील में बोल्सोनारो, अर्जेन्टीना में हावियेर मिलेइ, इत्यादि। आखिरकार, जैसा कि हेगेल ने इतिहास के दर्शनशास्त्र पर अपने व्याख्यानों में बताया था, “अनुभव और इतिहास यही सिखाता है — कि लोगों और सरकारों ने कभी भी इतिहास से कुछ नहीं सीखा है।” इस पूंजीवादी राजनीतिक चक्रव्यूह को भेदने का एक ही जरिया है — वह है इन चक्रव्यूहों के आधारभूत सामाजिक संबंधों, जो सत्ता को जनता से अलग कर उसे सत्ताधीन रखते हैं, पर क्रांतिकारी वार!